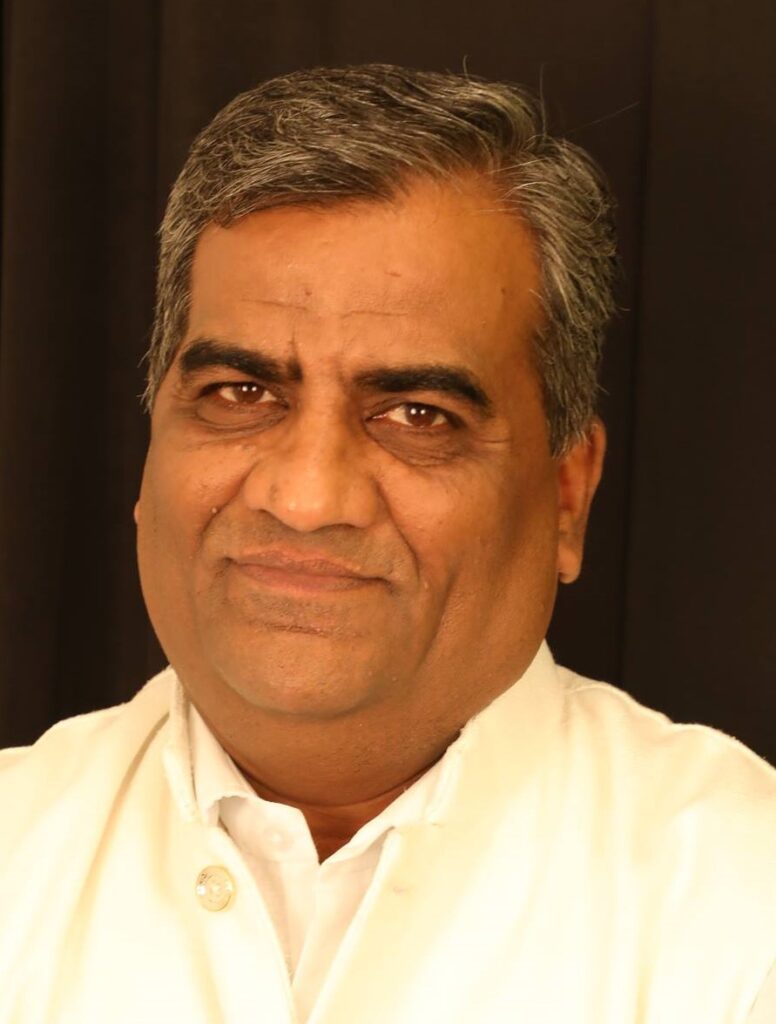
- राघवेंद्र तेलंग
सुपरिचित कवि,लेखक,विज्ञानवेत्ता
रूपांतरण की तरंगें और विदुषी सुलेखा भट के संगीत का प्रकाश
भारतीय मनीषा में प्रकृति शब्द का प्रयोग बहुत ही सजगता से अनेकानेक अर्थों में किया गया है। इस शब्द को सृष्टि, संसार, पर्यावरण, परिस्थिति, जन, गण, मन, शून्यता, अटल सत्य, मानस की अवस्था या स्वभाव आदि अन्य अर्थों में लिया जाता है। कहा जा सकता है कि इस तरह प्रकृति की परिभाषा अपने लिए पूरे ब्रह्माण्ड का ही प्रतीक बन जाती है। इस तरंगित कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा का उद्भव सूक्ष्म नाद से होकर जब अत्यंत व्यापकता में महसूस होता है तो यह विराट क्षेत्र सूक्ष्म का क्षेत्र बन जाता है। गीता में इस कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा के जानकार, वादक, गायक, कलाकार को क्षेत्रज्ञ की उपमा दी गई है। और क्वांटम लेवल पर यह संबोधन कृष्ण को जाकर छूता है।
संगीत रूपांतरित करता है। संगीत कायांतरण कर देता है। संगीत ऋतु परिवर्तन का एक आवश्यक औज़ार है, संकेतक है। संगीत पहले मुग्ध करता है फिर मंत्रमुग्ध करता है अंतत: संगीत आपमें ग्रेविटी पैदा कर देता है। संगीत आपके अंदर के चुम्बकत्व को जगाता है। संगीत तथा प्रकृति के अभिन्न सम्बन्ध को हम सब संवेदनशील मनुष्य होने के नाते महसूस करते ही है। सांगीतिक चेतना चहुंओर सभी में व्याप्त है। नदियों की कल-कल ध्वनि, हवा की सांय-सांय,सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट,हर तरफ हम संगीत की ध्वनि और लयात्मकता महसूस करते हैं। निसर्ग की ओर बिना पूर्वाग्रह के,बिना अपेक्षा के निहारने से हम एक प्रकार का कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा घटते हुए सुन पाते हैं। और यह दर्शित होता है झींगुरों के संगीत,पंछियों की बोली,जंतुओं और जीवों के विशेष सप्तक में गूंजते सुरों में।
जहां भी गति है वह और वहां संगीत है। आवृत्तियों का एक खेल समय के पिटारे के अंदर चल रहा है। जो इस खेल को खिला रहा है उसकी बीन पिटारे के बाहर है। वह झूमता है तो धरती कंपित होती है। उसके झूमने से संगीत है या कहें सब कुछ जो डोल रहा है उससे संगीत है,उसमें संगीत है। आवाज़ की तरंगों से मिलकर एक आंख तैयार होती है फिर ऐसे में देखकर भर ही डोलना हो जाता है। डोलते हुए एक तरंग में वह उतरता है जो हर दोलन का प्रणेता है।
जी हां! आज हंसध्वनि में एक ऐसी संगीत विभूति की बातें जिनके कंठ में सरस्वती विराजती हैं और किसना की मुरलिया हर श्रोता के भीतर उग आती है। लेकिन आज संगीत और संगीतकार को श्रोता के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान-विज्ञान की बातों से देखा-भाला जाएगा। ऐसा इसलिए कि फिलामेंट एलिमेंट जो वांछित है उसका एकमेव आऊटपुट रूपांतरण ही तो है। अब तक हंसध्वनि के विविध आलेखों के जरिए आपको अनुमान लग ही गया होगा कि रूपांतरण की आवृत्तियां विचार,कर्म और व्यवहार से मिलकर बनती हैं और आपकी जीवनशैली में प्रतिबिंबित होती हैं। इस प्रक्रिया से रूप और आत्मा एक ऐसे विनिर्दिष्ट बिंदु पर समांतर दीख पड़ते हैं कि दो रास्ते पर एक साथ चयनित-दृष्टि-विकल्प से यात्रा अग्रसर हो सकती मालूम पड़ती है।
हर रूपांतरण की क्रिया को यह तथ्य इतना शक्तिशाली बना देता है कि आप अपने में पर्सपेक्टिव या सोच को दो अलग-अलग तरीकों के बीच स्विच कर पाते हैं। विकल्पों भरी यात्रा में आनंद इस तरह प्रवेश करता है। टाइम के स्पेस में या कहें टाईम-स्पेस के फैब्रिक डोमेन को सतत तरंगित बनाए रखने वाली आवृत्ति डोमेन ही तो है जिसमें फैब्रिक के कारण पल पल में सिग्नल बदलता रहता है और और फलत: हर एनकोडेड सिग्नल शक्तिशाली होता चलता है,वह भी क्रिया,कारक या कर्ता के कारण। टाइम-स्पेस की स्लेट पर घटित होती आवृत्तियों को विश्लेषित करता दृष्टिकोण का यह बदलाव इसीलिए मायने रखता है।

जी हां! आज क्वांटम भौतिकी के बारीक दृष्टिकोण से संगीत के कुछ अनछुए पहलुओं पर एक सिंहावलोकन करने का प्रयास है। आज इस आलेख की प्रेरणा विभूति हैं प्रख्यात शास्त्रीय गायिका विदुषी सुलेखा भट। वरेण्य शास्त्रीय गायिका वीणा सहस्त्रबुद्धे प्रणीत गायकी और उनकी गुरू-शिष्य परंपरा की वाहक सुलेखा भट जी को मैंने कई बार ध्यानमग्न होकर सुना है और पाया है कि उनके वोकल म्यूजिक की प्रस्तुति के दौरान तरंगों का प्रोबेबलिस्टिक नृत्य डिजिटल प्रसंस्करण के विविध आयामों को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़े जाने पर नैसर्गिक की शक्ति की प्राण-प्रतिष्ठा स्वयंसिद्ध हो जाती है। स्पष्ट है तरंगों के नृत्य के बीच तरंगों के मिश्रण में संयोग और संभाविता के सभी पहलुओं का अध्ययन बिना क्वांटम कॉन्सटेंट तय किए संभव नहीं।
रैंडम आवृत्तियों की कांट-छांट करते चलना एक गायक के लिए तब और आसान हो जाता है जब उसके पास तीनों सप्तकों यानी ऑक्टेव पर पूरा नियंत्रण हो। सुलेखा भट जी की कुछेक लाइव प्रस्तुतियों का मैंने साक्षात् श्रवण किया है और मैंने पाया कि उनकी गायकी में मूल स्वर की आवाजाही के बीच तीनों सप्तकों की आवृत्तियों के बीच हर सप्तक की प्राकट्यता उन आवृत्तियों के हर सप्तक की प्राकट्यता उन आवृत्तियों के परस्पर संबद्ध अनुपातों में एक दिलचस्प लॉगेरिद्मिक क्रमबद्धता रिफ्लेक्ट होती है। इसके लिए उनका गाया संत चोखामेला का वह अभंग याद आता है जिसके बोल हैं जोहार माय बाप,जोहार माय बाप…।
जिस अनूठे पहलू की ओर मैं संकेत कर रहा हूं उसका आधुनिक तकनीक के संसार में सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग गणितीय उपकरणों में देखा जा सकता है, जिसे एमआरआई स्कैन से लेकर डिजिटल डॉल्बी सिस्टम के संगीत और छवि प्रसंस्करण यानी इमेज प्रोसेसिंग तक, हर चीज़ में अंतर्निहित गुण बतौर देखा जा सकता है।

समय डोमेन में यह देखते चलना कि पर्टिकुलर आवृत्ति का एक सिग्नल पल-पल कैसे बदलता है, लेकिन वही सिग्नल वेव्हलेंग्थ स्पेक्ट्रम के डोमेन में जब आप देखते हैं कि वहां कितनी तो कॉम्बिनेशनल आवृत्तियाँ मौजूद हैं और प्रत्येक कितनी प्रबल है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ज़िप तकनीक से छवियों की बड़ी फाइलों को कम्प्रेस यानी संपीड़ित करने और सिग्नल टू नॉइज़ रेश्यो के मद्देनज़र शोर वाले ऑडियो को फिल्टर या साफ़ करने और यहाँ तक कि श्रवण का यह पहलू डेटा में दोहराए जाने वाले पैटर्न का पता लगाने में किसी भी डिजिटल उपकरण को सक्षम बनाता है। अगर यह सब जटिल लग रहा हो तो सीधी बात कह ही दूं कि जिस प्रकार एक संगीतिक राग को विभिन्न स्वरों के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है, उसी प्रकार किसी भी दोहराए जाने वाले या उतार-चढ़ाव वाले सिग्नल को सरल साइन और कोसाइन तरंगों के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसे विभिन्न सप्तकों से गुज़ारते हुए श्रोता के लाइव कोसाइंस में से होते हुए स्वर-रसास्वादन को फिल्टरेशन की अनुभूति के जरिए संपन्न कराया जाता है।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सांगीतिक डोमेन में राग की छवि का रूपांतरण का कीमिया एक गणितीय प्रक्रिया है जो एक जटिल सिग्नल को उसके मूल आवृत्ति घटकों में विभाजित करता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि छानने की प्रक्रिया को लगातार बदलती छन्नियों को एक निश्चित पैटर्न में बारम्बार दोहराते हुए अंतत: उसके मूल स्वर की आवृत्ति तक पहुंच जाना ही वह बारीक सूत्र है। समय के साथ बदलने वाले हर तरह के ऑर्केस्ट्रा की सांगीतिक लयात्मकता को छानते चले जाने से इनपुट का कोई भी सिग्नल चाहे फिर वह ध्वनि तरंग हो या दृश्यात्मक वीडियो या छवि पैटर्न या इको-कार्डियोग्राफ में हृदय गति के संकेत हो,यह प्रक्रम उसमें छिपे ‘स्वर’ या आवृत्तियों को प्रकट करता है और तब यह उसके मूल या जड़ की आवृत्ति का आस्वाद होता है।
@ इस आलेख के सर्वाधिकार लेखकाधीन सुरक्षित हैं।
raghvendratelang6938@gmail.com

