‘भक्तिवाद और भक्ति’: ‘आधुनिकता और रूमानियत’
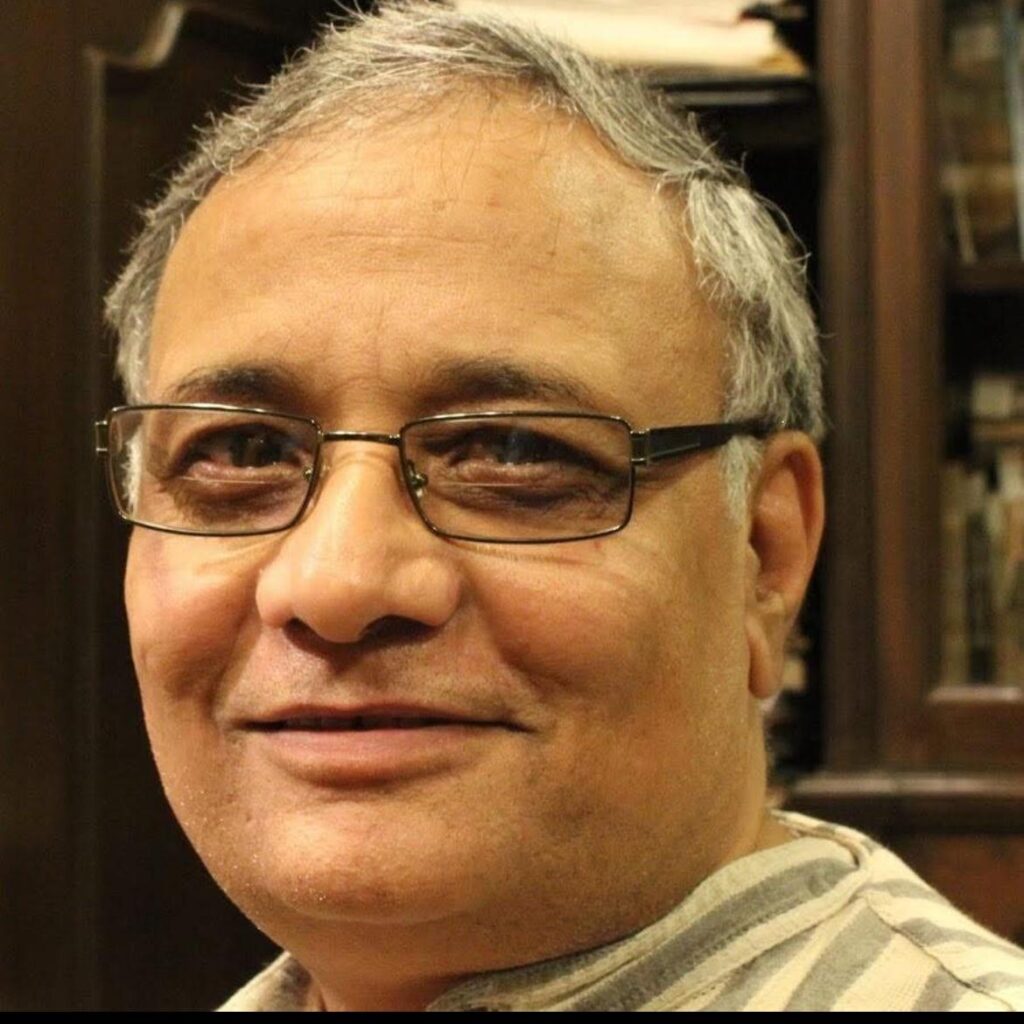
- अरुण माहेश्वरी
प्रख्यात मार्क्सवादी चिंतक और लेखक
1 फरवरी के टेलिग्राफ में प्रसिद्ध भाषा शास्त्री जी.एन. देवी का एक लेख है– ‘मध्ययुग अंधकार का काल नहीं था: भक्तों के बजाय भक्ति।’
श्री देवी पहले भी अपनी पुस्तकों और लेखों में भारत के सामाजिक इतिहास के त्रिकालीय (प्राचीन, मध्य और आधुनिक युग) विभाजन की सच्चाई को सर विलियम जोन्स से शुरू करके औपनिवेशिक इतिहासकारों की कल्पना की उपज बता कर सत्तर्क खारिज करते रहे हैं। इस लेख में अपने उसी विवेचन की श्रृंखला में उन्होंने फिर एक बार उस मध्ययुग और भक्ति काल को अपना विषय बनाया है जो युग न सिर्फ सभी भारतीय भाषाओं के उदय का युग था बल्कि उनके अनुसार ‘भक्ति’ के एक सूत्र से संपूर्ण भारत को ‘प्रेम और विद्रोह’ के मानवीय भावों के एक सूत्र से बांधने वाला वैसा ही युग था जैसा कि यूरोप में रूमानियत और आधुनिकता के युग में पाया जाता है।
श्री देवी ने अपने इस लेख में दिखाया है कि कैसे ‘भक्ति’ पद भारत की सभी भाषाओं में एक साथ, समान अर्थ में पाया जाता है। तमिल में सिर्फ इतना सा फर्क आया है कि यह भक्ति के बजाय पक्ति या पक्ते हो गया है। उन्होंने भक्ति के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाले devotion शब्द को अनुपयुक्त माना है क्योंकि devotion से जिस प्रकार की निष्ठा और वफादारी की ध्वनि मिलती है, उनके अनुसार भक्ति से तात्पर्य उसके बजाय ऐसे निःस्वार्थ उत्सर्ग (selfless surrender) से हैं जो आनंददायी होता है। श्री देवी ने बिल्कुल सही भक्ति पद की व्युत्पत्ति को ‘भज’ से जोड़ते हुए लिखा है कि उसके अर्थ को भागीदारी, हिस्सेदारी से जोड़ कर अपना यह विमर्श तैयार किया है।
जाहिर है कि श्री देवी का यह प्रयास एक प्रकार से भक्ति को हर रूढ़ि और अंध समर्पण से मुक्त करके उसे प्रेम भाव के मानवीय तत्त्व से जोड़ने का है और इसी अर्थ में वे भक्ति की अखिल भारतीय व्याप्ति की तुलना साहित्य के इतिहास में ‘रूमानी’ अथवा ‘आधुनिक’ से करते हैं। भक्ति की परंपरा को कथित मध्ययुग के मीरा, कबीर तक सीमित रखने के बजाय आधुनिक काल के रवींद्रनाथ, महात्मा गांधी और डॉ.अंबेडकर तक खींच लाते हैं।
बहरहाल, यहां हम विषय को थोड़ा अलग कोण से देखना चाहते हैं। श्री देवी की इस टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य आज के मनुष्य के सामने सर्वनाश की मौजूदा परिस्थितियों से मुक्ति के रास्ते की तलाश रही है जिसमें वे यूरोपीय मानवतावाद की भांति ही भारत के भक्ति आंदोलन में अपार संभावना देखते हैं और इसी उद्देश्य से वे भक्ति की मूल रूमानी, आनंददायी धारणा को आज के ‘भक्तों’ की उद्दंडताओं से अलग करते हैं।
अपनी टिप्पणी में श्री देवी जहां वर्तमान में सभ्यता के व्यापक संकट के संदर्भ में भारतीय समाज में भक्ति पद की व्युत्पत्ति और भक्ति आंदोलन को देख रहे हैं, वहीं हम भी आज के भारत में सांप्रदायिक फासीवाद के संदर्भ में धर्म और उससे जुड़े ‘भक्ति’ के सच को टटोलना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि यूरोप में जहां ‘रूमानियत’ और ‘आधुनिकता’ की धारणा में धर्म और धार्मिक रूढ़िवाद का कोई स्थान नहीं है, वहीं भारत में ‘रूमानियत’ और ‘आधुनिकता’ के कथित समानार्थी ‘भक्ति’ की धर्म और संप्रदाय तथा उनसे जुड़ी राजनीति में प्रमुख भूमिका क्यों और कैसे हैं ?
श्री देवी ने अपने सामाजिक मंतव्य के लिए शब्दानुशासन का प्रयोग करते हुए ‘भज’ शब्द से ‘भक्ति’ पद की व्युत्पत्ति के आधार पर ही इसके भागीदारी, हिस्सेदारी के अर्थ को रेखांकित किया है। हम भी यहां इस पूरे विषय को शब्दानुशासन, भाषा विज्ञान और सौन्दर्यशास्त्र के मानदंडों पर ही विवेचित करना चाहते हैं। अपने इस विवेचन का एक बहुत उपयुक्त सूत्र हमें आनंदवर्धन के ‘ध्वन्यालोक’ और उस पर अभिनवगुप्त के लोचन से मिलता है। ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा बताते हुए ध्वनि सिद्धांत की स्थापना जिन ध्वनि-विरोधी मतों के खंडन के आधार पर की है, उनमें एक प्रमुख धारा ‘भक्तिवाद’ की पाई जाती है।
आनंदवर्धन ने अपने ध्वनि-सिद्धांत में यह बताया था कि काव्य में मुख्यतः तीन प्रकार की अर्थव्यंजना पाई जाती है: अभिधा (शाब्दिक अर्थ), लक्षणा (प्रसंगानुसार व्यंजित अर्थ) और व्यंजना (गूढ़, अप्रत्यक्ष या ध्वनि-सिद्ध अर्थ)। उनका मानना था कि श्रेष्ठ काव्य वही होता है जिसमें व्यंजना (ध्वनि) प्रधान होती है। इस सिलसिले में उन्होंने ध्वनि-विरोधियों को तीन प्रमुख धाराओं की पहचान की: अभिहितान्वयवाद – जो मानते थे कि काव्य में केवल अभिधा (शाब्दिक अर्थ) ही मायने रखती है; अनुमेयवाद – जो मानते थे कि काव्य का प्रभाव तर्क (अनुमान) से जाना जाता है; और भक्तिवाद – जो मानते थे कि काव्य में लक्षणा ही पर्याप्त है, व्यंजना या ध्वनि को अलग से मान्यता देने की जरूरत नहीं है।
इनमे भक्तिवाद का तर्क था कि जब कोई शब्द अपने प्रत्यक्ष अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, तब वह ‘लक्षणा’ से अपना दूसरा अर्थ ग्रहण करता है। लेकिन काव्य में कोई ‘अतिरिक्त व्यंजना’ (ध्वनि) नहीं होती; इसी आधार पर ध्वनि सिद्धांत को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।
जाहिर है कि इस दृष्टिकोण में ‘भक्ति’ का अर्थ है – शब्द को उसके प्राथमिक अर्थ से हटाकर लक्षणा के माध्यम से समझना। इस दृष्टि से, भक्ति की धारणा की व्युत्पत्ति (भज्, अर्थात् विभाजन, समर्पण, आश्रय) भाषा के उस प्रयोग को संकेतित करती है जिसमें शब्द अपने प्रत्यक्ष अर्थ से हटकर एक माध्यमिक आश्रय (लक्षणा) ग्रहण करता है, लेकिन ध्वनि (व्यंजना) को अस्वीकार करता है। यही भक्तिवाद की केंद्रीय अवधारणा थी। जहां तक ‘भज’ के अर्थ के रूप में हिस्सेदारी, भागीदारी का सवाल है, यह अर्थ पाणिनि की अष्टाध्यायी और यास्क के निघंटु तथा निरुक्त में मिलता है − हिस्सेदारी, भागीदारी और समर्पण, जबकि संस्कृत मूल के भज धातु से निकले भक्ति का अर्थ सेवा करना, समर्पण करना, किसी के प्रति विशेष अनुराग रखना होता है। ‘समर्पण’ दोनों जगह पर पाया जाता है। आनंदवर्धन जिस भक्तिवाद का खंडन करते हैं उसमें भक्ति वह प्रयोग है जो आश्रय पर निर्भरशील होती है। उसके अनुसार शब्द ‘लक्षणा’ में समर्पित होता है और वही पर्याप्त है। इससे अलग कोई व्यंजना शक्ति नहीं होनी चाहिए।
भक्तिवाद इसीलिए ध्वनि-सिद्धांत का विरोध करता है कि वह भाषा को स्वतंत्र ध्वनि या अप्रत्यक्ष व्यंजना के आधार पर नहीं, बल्कि केवल प्रकट लक्षणा पर निर्भर मानता है। इस दृष्टिकोण से भक्तिवादियों ने साहित्य में ध्वनि (व्यंजना) की स्वतंत्र सत्ता को नकारा था।
जाहिर है कि आनंदवर्धन ने ध्वनि-विरोधी धारा के रूप में जिस ‘भक्तिवाद’ का खंडन किया था, वह कोई धार्मिक प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि काव्य-चिंतन की एक विशिष्ट विरोधी धारा थी। यह धारा भाषा को सिर्फ अभिधा और लक्षणा तक सीमित रखना चाहती थी, जबकि आनंदवर्धन और बाद में अभिनवगुप्त ने यह स्थापित किया कि काव्य में व्यंजना (ध्वनि) एक स्वतंत्र शक्ति होती है, जो अर्थ को गहराई प्रदान करती है।
इस प्रकार यह साफ़ है कि भाषा की दृष्टि से भक्ति में व्यंजना से इंकार संपूर्ण भक्ति-भाव में एक प्रकार की रूढ़ता के भाव को स्थापित करता है। आनंदवर्धन के ध्वनि-सिद्धांत का मूल तर्क यह था कि सर्वोत्तम काव्य में व्यंजना (suggestion) की भूमिका होती है, जो पाठक या श्रोता को शब्दों के प्रत्यक्ष और लाक्षणिक अर्थों से आगे जाने की अनुमति देती है। लेकिन भक्तिवादियों ने इसे अस्वीकार किया और केवल अभिधा (शाब्दिक अर्थ) और लक्षणा (माध्यमिक, संदर्भित अर्थ) तक काव्य की व्याख्या को सीमित रखा। भक्तिवाद के दृष्टिकोण से काव्य केवल लाक्षणिक रूप तक सीमित रह जाता है। यह श्रद्धातिशयता शब्दों की व्याख्या को एक निश्चित दायरे में बंद कर देता है और पाठक को काव्य में अंतर्निहित गूढ़ अर्थों तक पहुँचने से रोकता है। इसके कारण काव्य-विचार एक स्थिर (static) प्रक्रिया बन जाती है, जिसमें नए अर्थों की संभावना समाप्त हो जाती है।
कहना न होगा, भक्ति के संपूर्ण भाव में भी यही रूढ़ि परिलक्षित होती है। धार्मिक एवं साहित्यिक अर्थों में भक्ति एक निश्चित
आस्था की माँग करती है, जिसमें प्रश्न करने या नए अर्थों की खोज की गुंजाइश कम होती है। जैसे भक्तिवाद में काव्य-विचार को व्यंजना से दूर रखने की प्रवृत्ति भाषा की संभावनाओं को सीमित कर देती है, उसी प्रकार, धार्मिक भक्ति में भी संदेह या आलोचना के लिए जगह नहीं होती है।
ध्वनि-सिद्धांत गतिशीलता का समर्थन करता है, क्योंकि इसमें पाठक के लिए नए अर्थों को खोजने की स्वतंत्रता रहती है। इसके विपरीत, भक्तिवाद एक स्थिर संरचना की ओर जाता है, जिसमें व्यंजना को अस्वीकार करने से काव्य को निश्चित अर्थों तक सीमित कर दिया जाता है। भक्तिवाद में व्यंजना के अस्वीकार से भक्ति की अवधारणा में एक प्रकार की जड़ता (rigidity) आती है, जो भाषा और साहित्य की गतिशीलता को सीमित कर सकती है। यह प्रवृत्ति काव्य की बहुअर्थीयता और उसकी संभावनाओं को संकुचित कर देती है, जिससे साहित्यिक अभिव्यक्ति में रूढ़ता का भाव प्रवेश करता है। इसीलिए, यही कहना उचित होगा कि भक्तिवाद की प्रवृत्ति, चाहे वह साहित्यिक हो या धार्मिक, व्यंजना से इनकार करने के कारण एक प्रकार की रूढ़ता स्थापित करती है।
इस प्रकार, जब हम भाषा संबंधी इस पूरे विमर्श की रोशनी में भक्तिवाद की परंपरा को देखते हैं तब निश्चय ही हम श्री देवी की तरह रवींद्रनाथ और डॉ. अंबेडकर के स्तर के आधुनिक चिंतकों और गांधी के स्तर के धर्म-निरपेक्ष समाज सुधार के जन-नेता को भक्ति के किसी भी मूलगामी, रूढ़िवादी अर्थ से नहीं जोड़ पाते हैं। इस विषय पर हम साफ तौर पर श्री देवी के विचारों से मतभेद व्यक्त करते हैं।

