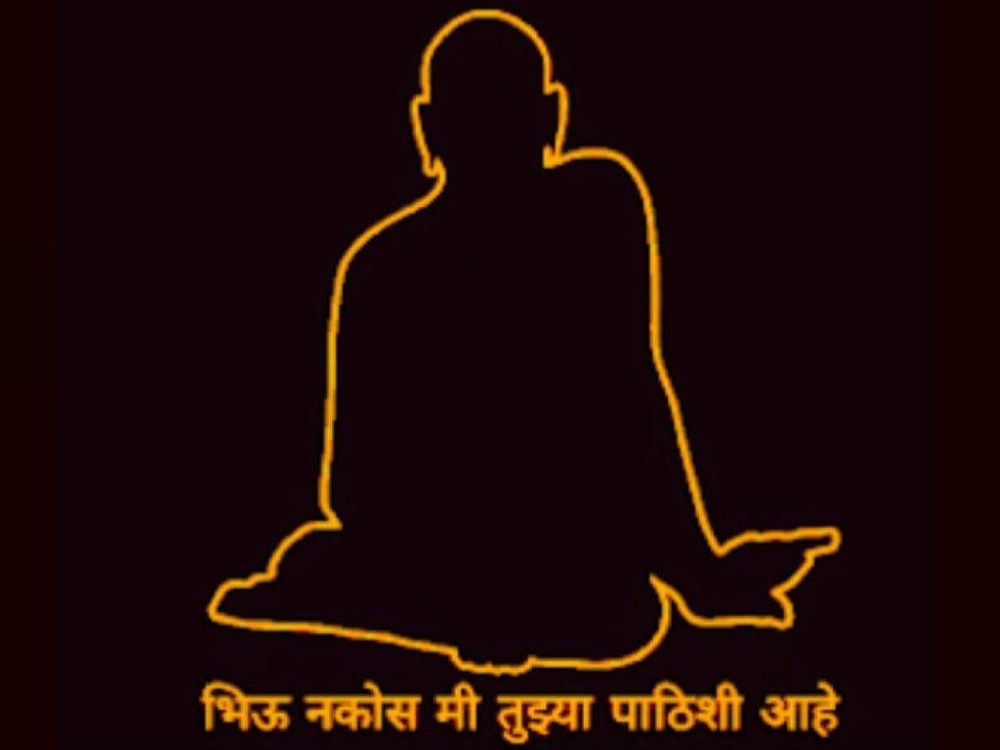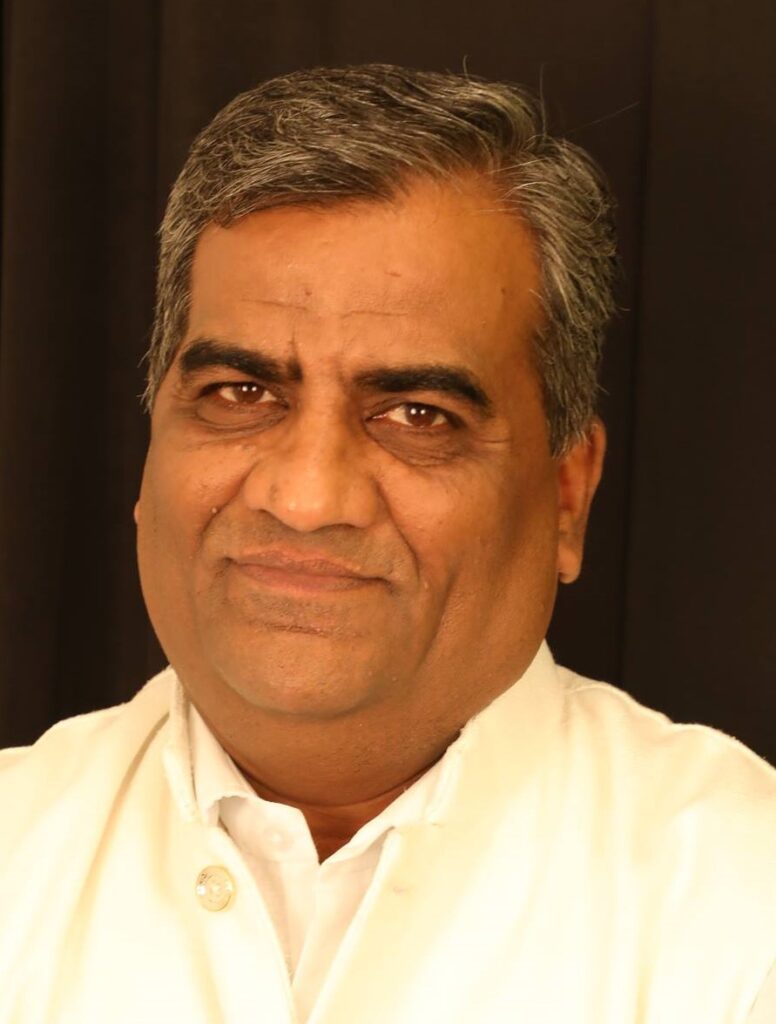
- राघवेंद्र तेलंग
सुपरिचित कवि,लेखक,विज्ञानवेत्ता
पहली बात तो यह कि यह सब जो यहां लिखा जा रहा है वह ईश्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह कि यह स्तुति न होकर माहात्म्य की विवेचना है।
फिर लिखता हूं कि यह सब लिखना दर्शित मूर्ति रूप उस ईश्वर के बारे में नहीं है। और न ही यह उस ज़माने के बारे में है जब सड़क परिवहन निगम की बस में ड्राइवर के ठीक पीछे सवारियों की नज़रों की दिशा में लिखा होता था कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। हां!,शीर्षक का यह विचार अवश्य वहीं से लिया गया है।
यह सब जो लिखा जा रहा है वह उस ईश्वर के बारे में है जो विचार में आते ही आपकी यात्रा में भी शामिल हो जाता है। सोचकर देखिए! यात्रा में एक बार बगल में किसी की नेविगेटर सीट पर अगर ईश्वर सहयात्री के रूप में बैठ जाए तो फिर उस सफर को तो तब सफल होना ही है।
ईश्वर एक नाम के परसेप्शन के रूप में जैसे ही भीतर उतर आता है,आपका अकेलापन दूर हो जाता है। और जब आपका अकेलापन जाता रहता है तब भय के उस स्थान पर साहस अपने सूक्ष्म रूप में आ विराजमान होता है,जिसके बूते समूची यात्रा संपन्न होती है। एक बार शक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को आपके भीतर कंसीव्ह होने भर की देर है फिर उसके बाद सूक्ष्म की विराट शक्ति का काम शुरू हो जाता है और वह भी कुछ इस तरह कि वह शक्तिपुंज आपको सदा स्मरण दिलाता चलता है कि दुर्घटना की आशंका वाले पलों में आपकी सुरक्षा के लिए आपका यह सबसे विश्वसनीय साथी आपके साथ है।
जब यह लिख रहा हूं तब मेरे घर में एक तस्वीर पर स्वामी समर्थ महाराज का आशीर्वचन दृष्टव्य है कि घाबरू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे! (अर्थात! घबरा मत मैं तेरे पीछे खड़ा हूं!)। इस वाक्यांश की ध्वनि के अर्थ भी इसी संदर्भ को संप्रेषित करते हैं। यह जानना आपको दिलचस्प लगेगा कि मेरे काम से जुड़े मेरे सभी पसंदीदा स्थान वही हैं जहां आस्था-विश्वास की सांकेतिक तस्वीरें या प्रतीक चिह्न लगे होते हैं। फिर वह जगह चाहे जूतों की मरम्मत करने वाले की हो, कपड़े प्रेस करवाने की हो या हो किराने की दुकान या फिर वह इस ऑनलाईन पोर्टल ‘टॉक थ्रू’ के ऑफिस में संपादक महोदय की कुर्सी के पीछे टंगा ज़ेन दर्शन एनसो की कलाकृति ही क्यों न हो।
हंसध्वनि के इस मंच में कई बार दोहराया जा चुका है कि ईश्वर परसेप्शन ऑफ परसेप्शंस की बात है और इसीलिए वह एक जो सर्वलोकैकनाथम है, एक साथ कई लोगों के परसेप्शन में वास करता है। वह एक सबको सुलभ भी इसीलिए है क्योंकि वह मुक्त ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा को मानव रूपी कुम्हार किसी भी फॉर्म में अपने परसेप्शन के जरिए अपने जीवन में प्रयोग में ला सकता है। आज के समय में विचारों की बाढ़ से हम इतने आक्रांत हैं कि आमूलचूल बदलाव लाने के लिए नए सिरे से शून्यवत होकर शुरूआत करना होगी। निश्चित ही विचारहीन अवस्था यानी ज़ीरो प्वांइट पर जाकर अपनी मौलिकता पुन: हासिल कर ही फिर नवोदय हो सकेगा। बताता चलूं कि ईश्वर सघन मौन के कुएं में ही वहां गहरे करीब जाकर मिलता है जहां उसके पास और कोई दूसरा नहीं होता।
मौन ईश्वर की यूनिवर्सल भाषा है,जो वर्णमाला से मुक्त है। वहीं दूसरी ओर शोर मनुष्य की ईजाद की हुई भाषा है। सुख का संसार ध्वनि के अनुपात के गणित का परिवृत्त है। दस प्रतिशत कानों से टकराता भाषा का शोर और नब्बे प्रतिशत शरीर में से आती-जाती मौन की आवृत्तियां। जिस तरह समूचा जीवन सही अनुपात को साधने की कवायद है वैसे ही जीवन को संगीतमय बनाना विषम और सम के अनुपात को साधने से संभव हो पाता है।
ईश्वर की अवधारणा मानव की जीवन प्रणाली में ऑक्सीजन की तरह काम करती है। ईश्वर का नकार अपने अस्तित्व के निर्माता और उसके बनाए अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करना है। यह कुछ ऐसा है कि आप दिखाई देने वाली हर जड़ चीज़ पर तो विश्वास करते हैं पर उन चीज़ों में समाई और उन्हें ऑपरेट करने वाली अदृश्य ऊर्जा पर विश्वास नहीं करते। मेरा इशारा साइंस और गणित के अंधमोह में आकंठ डूबे बौद्धिकों की ओर हैं। ये तथाकथित हर संरचना को शक्की दृष्टि से देखते हैं ताकि उसका विखंडन कर नये निर्माण का दु:स्वप्न पूरा कर सकें। ये भूल जाते हैं कि विखंडन के बराबर की ऊर्जा ही संलयन या नव निर्माण में लगती है और एक ही जीवन में दोनों तरह की ऊर्जाओं के प्रयोग का बोध कभी भी किसी एक के पास नहीं हुआ है। ऐसे विखंडनकारी तत्व अंतत: अश्वत्थामा की गति को प्राप्त हुए हैं।
ईश्वर के विचार की स्मृति खो जाने पर आपका संपर्क अस्तित्व से टूट जाता है। फिर नाभिक विहीन, दिशाहीन यात्राएं और नितांत भटकन ही भटकन हिस्से में आतीं हैं। ऐसे लोग फिर विखंडन की ऊर्जा के पक्ष में आजीवन काम करते पाए जाते हैं। निष्पक्ष का भाव इनके कल्पनालोक का विषय कभी नहीं बन पाता। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाकर आगे बढ़ जाना चाहिए।

ईश्वर का पहला विचार ऊर्जस्वित, नए और ताजातरीन बच्चे की तरह है जो जा-जाकर सब पुराने पारिवारिक सदस्यों को जोड़ता है। इसीलिए हमने विचार को चेन रिएक्शन की प्रकृति का-सा कहा।
जे. कृष्णमूर्ति सहित ऐसे अनेक विचारक हुए हैं जो विचार के दर्शन और विचार के असर के कीमिया को बारीकी से समझाते हैं। आपका हर विचार आपका है,फिर यह चाहे भीतर के अंतरंग से उपजा हुआ विचार हो या फिर बाहर के बहिरंग से उपजाया हुआ विचार। प्रश्न सिर्फ यह है कि आप उसको अपने हित में कैसे बरतते हैं,हैंडल कैसे करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि विचार एक इंजन प्रणाली है या घोड़ा है जो अपने सवार को सैर भी करा सकता है या फिर उसे ही बेकाबू ढंग से चलायमान कर पीठ से गिरा भी सकता है।
हर विचार एक चेन रिएक्शन को जन्म देता है। इसीलिए विचार के पनपते ही उसे चैनलाइज़्ड सर्किट में यानी एक उद्देश्यपूर्ण हित में झोंक देना चाहिए। ऐसा न करने पर कोई भी विचार अपनी रैंडमनेस प्रकृति के कारण सब कुछ तहस-नहस करने की शक्ति रखता है। विचार के नियंत्रणकर्ता यानी ड्राइवर ही आपको इस विचार के प्रति तैयार करते हैं कि जीवन डायनामिक है,चलता हुआ सतत और इसके साथ ही हर यात्रा में बराबर जोखिम भी यात्रा करता है,संतुलन के प्राकृतिक नियम के अंतर्गत। दु:ख और सुख हमारे जुड़वां साथी हैं,इस तथ्य की समझ यात्रा से ही अनुभूत होती है।
हम कहीं भी निकलते हैं। हम घर से निकलते हैं। हम अपने में से बाहर निकलते हैं। हम घर के अंदर प्रतिष्ठापित ईश्वर को सकुशलता की प्रार्थना,नमस्कार करके निकलते हैं। हम घर से सलामत लौट आने की एक दुआ के साथ निकलते हैं। ज्यादातर अवसरों पर हम सही-सलामत लौट आते हैं और लौटकर भले ही हम ईश्वर का धन्यवाद कहना भूल जाते हों पर यह हमारे यकीन में रहता है कि ईश्वर हम सबकी हर यात्रा सफल करता है। जीवन की यात्रा में यह जादुई वाक्य हर जगह सफल पाया गया है। दिलचस्प है यह समझना कि इस वाक्य की सफलता में आपके उस परसेप्शन ऑफ परसेप्शंस का बड़ा हाथ है जो उस ड्राइवर के अमूर्त रूप को भी अपना हिस्सा मानता है जिसकी पीठ के पीछे लिखा है:
‘ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे!’
raghvendratelang6938@gmail.com