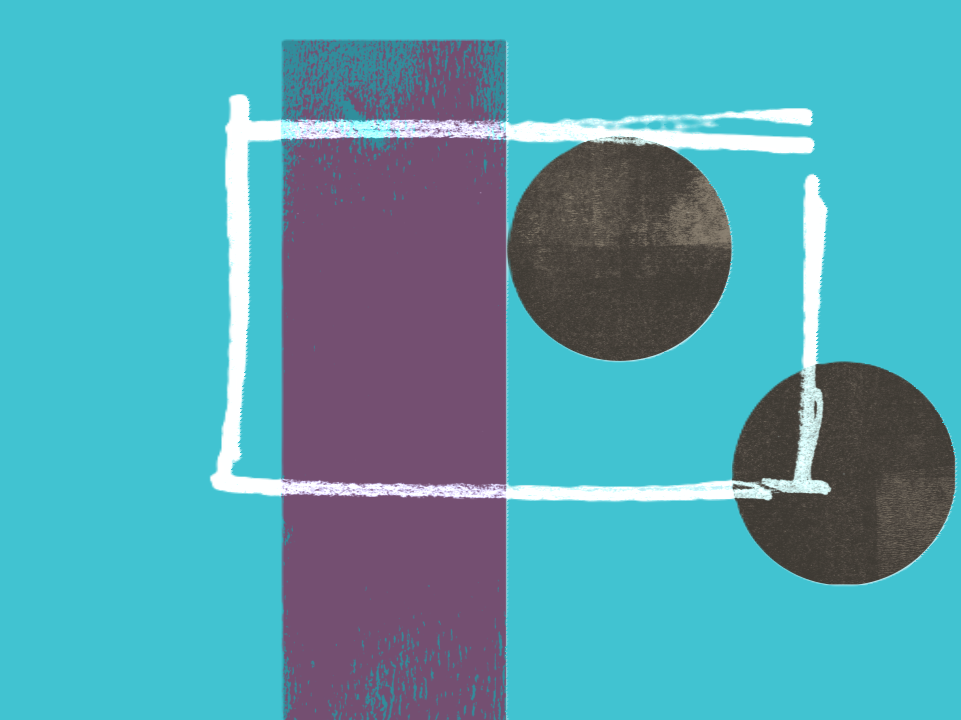चैतन्य नागर, स्वतंत्र पत्रकार
लगभग हर मां आमतौर पर ऐसा बेटा चाहती है, जो उसपर, बस उसी पर जान छिडकता हो। वही मां जब पत्नी थी, तब वह चाहती थी कि उसका पति अपनी मां का नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका ख्याल रखे। मां यह भी चाहती है कि उसका दामाद उसकी बेटी का ख्याल रखे अपनी मां का नहीं, पर उसका बेटा अपनी पत्नी का ख्याल कम रखे उसका ज्यादा। ये रिश्तों की सियासत है; इसकी विरोधाभासी मांगें हैं।
खासकर भारतीय समाज में पुत्र एक युद्धभूमि में परिवर्तित हो जाता है, और इस युद्धभूमि पर एक ओर माता अपने अपने शास्त्र और शस्त्रों के साथ, और दूसरी ओर पत्नी विचारों और भावनाओं की सेना के साथ एक दूसरे पर निशाना साधे रहती हैं। मानव संबंध तो जटिल होते ही हैं पर जितनी जटिलता इस संबंध में अभिव्यक्त होती है, वह तो अद्भुत और असाधारण होती है! उसकी कोई तुलना ही नहीं! ऐसे कितने ही पुत्र आपने देखे होंगे जिनके जीवन का अच्छा ख़ासा समय बीतता है परिवार के इन दो सत्ता केन्द्रों के बीच संतुलन कायम करने में!
‘मम्माज बॉयज’ (मां के लाडले बेटे) बीवियों के बीच सबसे कम लोकप्रिय होते हैं। उनके लिए आफत भी होते हैं। आपको दो उदाहरण दूंगा और जो आपको बताएंगे कि किस तरह ‘मां का प्यार’ बच्चों के जीवन में बाधा भी खड़ी कर सकता है। इसमें एक तो किस्सा है प्रशासनिक सेवा के एक बड़े अधिकारी का। इन्हें दो पत्नियां सिर्फ इसलिए छोड़ गईं क्योंकि जब भी यह दफ्तर से घर आ पाते थे, अपने व्यस्त कार्यक्रम के बाद, तो इनकी माताजी इनसे कहती थीं कि वह उनके साथ ही बैठ कर चाय पियें। अधिकारी महोदय माता के प्रेम में डूब कर उनकी बात मानते थे रहे और नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक दोनों पत्नियां यह कह कर उन्हें छोड़ गईं कि आप अपनी माता के साथ ही रहें तो बेहतर होगा।
दूसरा मामला एक वैज्ञानिक का है। वैज्ञानिक महोदय यूरोप के किसी समृद्ध देश में बहुत अच्छे वैज्ञानिक बने काम कर रहे थे पर उत्तर भारत के एक प्राचीन नगर में वास कर रही उनकी माता ने कहा कि वह उसके पास नहीं जा सकतीं क्योंकि किसी भी हाल में वह अपने कुल देवता के मंदिर में पूजा करना और गंगा स्नान करना त्याग नहीं सकतीं। नतीजा यह हुआ कि बेटा अपना विज्ञानं और शोध वगैरह त्याग कर अपनी माता को पूजा और गंगा स्नान कराने वापस आ गया और अब वह एक आदर्श, महान पुत्र के रूप में जाना जाता है। यह बात अलहदा है कि इस महान देश में उस स्तर के वैज्ञानिक के लिए कोई साधारण सी नौकरी ढूंढना भी एवरेस्ट पर चढ़ने के सामान है। उसे अपने पुत्र के कर्त्तव्य और अपनी आर्थिक-सामाजिक जरुरत के बीच जैसे-तैसे संतुलन बनाना है, और उम्मीद है कि इस देश की उदार, उर्वरा भूमि पर उसे भी कहीं न कहीं कोई ठांव जरुर मिलेगी। पर माता-प्रेम के ये भी परिणाम हैं, इस पर गौर करना चाहिए। प्रेम चाहे जिसका हो, स्वार्थी होता है, और माँ का प्रेम कोई अलग किस्म का होता है, यह सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी भी हो सकती है।
कुदरत में मां की एक जैविक भूमिका है। वह बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, और जन्म के बाद उसे पोषण देती है। जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता और खुद से अपना भोजन नहीं जुटा पाता, मां उसकी देखभाल करती है। मानव शिशु की मां पर निर्भरता जैविक से अधिक सामाजिक कारणों से है। उसे ‘बड़ा करना, शिक्षित करना, उसका विवाह करना’ यह सब कुछ मां-बाप के सामाजिक ‘कर्तव्यों’ में शामिल है, और इसलिए इंसान के बच्चे को करीब जीवन के बीस वर्ष तक भौतिक रूप से मां-बाप पर निर्भर करना पड़ता है और इस दौरान उसके मानसिक और मनोवैज्ञानिक संस्कार ऐसे गहरे बैठ जाते हैं कि वह आजीवन मां-बाप पर और मां-बाप आजीवन उसपर लदे रह जाते हैं। समाज के वृहत्तर उद्देश्य के लिए काम करने में भी परिवार और मां-बाप आड़े आते हैं, यह हमारे सामाजिक जीवन की सच्चाई है।
मां का अनावश्यक, अतिरंजित महिमामंडन जितना इस देश में है, उतना कहीं नहीं। पर मां एक इंसान ही है, जैसे कि पिता. उसकी भी अपनी मजबूरियां, अपने दबाव हैं, संस्कार और असुरक्षाएं हैं। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की वजह से वह बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताती है और इस कारण समय पर आधारित लगाव भी उसे ज्यादा महसूस होता है। पर घर में रह कर बच्चों के खाने-पीने की हर वक़्त फिक्र करने वाली मां और घर से बाहर जाकर पूरे दिन नौकरी करने वाली मां में बहुत फर्क हो गया है। आधुनिक मां, पिता की तरह ही व्यस्त है। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और अपने सपने हैं। उसके ख्वाब अपने बच्चों के साथ जुड़े हों जरुरी नहीं। आधुनिक एकल परिवार और सब न्यूक्लियर परिवार (उप एकल परिवार) में पिता और माता दोनों सामान रूप से बच्चों की ज़िम्मेदारी निभाते हैं, या परिस्थितियां उन्हें बाध्य करती हैं और श्रम का परंपरागत विभाजन कायम नहीं रह पाता। अक्सर पिता भी माँ की परंपरागत भूमिका निभाता है।
यदि मां सही ढंग से शिक्षित है तो उसके बच्चे भी एक ऐसा जीवन जी पाएंगें जिसमें प्रज्ञा और अच्छाई दोनों हो। यदि वह खुद में उलझी हुई है, जीवन के बारे में कोई स्पष्ट समझ उसमे विकसित नहीं हो पाई है तो फिर उसका बच्चों पर असर उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना किसी भी अन्य बाहरी एजेंसी का। अधिकतर मां-बाप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि उन्हें बच्चों से प्यार नहीं। वह बच्चों को समाज के हिसाब से ‘सामान्य’ बनाना चाहते हैं और समाज खुद ही असामान्य है! यह हमारे समय के विरोधाभासों में है। एक असामान्य समाज के हिसाब से ताल मेल बैठा कर चलना ही असामान्य होना है।
यदि मां या पिता सिर्फ समाज के एजेंट हैं तो वह सच्चे अर्थ में मां-बाप कहलाने के लायक ही नहीं। वे एक विशाल पहिये की तीली भर हैं और अपने बच्चों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वे भी समाज नाम के उस पहिये की तीली बन कर रह जाएं। यदि कोई सही ढंग से अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहेगा तो फिर वह उसे जातिवाद, धार्मिक रुढियों, धर्मांधता और युद्ध की क्रूरता से परिचित कराएगा। ऐसे मां-बाप अपने बच्चों को सैनिक बनाने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे। वह नहीं कहेंगे कि उनका बच्चा किसी भी वजह से दूसरे इंसान की हत्या करे। पर वर्तमान सामाजिक ढाँचे की दुहाई देकर हम यही सब करते हैं।
बच्चों को आज्ञाकारिता नहीं, प्रश्न पूछना सिखाना चाहिए। प्रश्न पूछना उद्दंडता नहीं। उसका भी अपना अनुशासन होता है। जो मां-बाप कहें, वही सही नहीं होता। मां-बाप कोई सत्यान्वेषी नहीं होते। मां-बाप और बच्चे एक साथ जीवन की यात्रा के सहयात्री होते हैं और उनकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। अक्सर बच्चे अपनी नई उर्जा और अतीत के कम दबाव के कारण जीवन को ज्यादा साफ देखने की क्षमता रखते हैं और ऐसे में वे मां-बाप से ज्यादा सही होते हैं।
समय के साथ मां भी बदली है। बच्चे स्कूल से लौटें तो जरुरी नहीं कि मां दरवाजे पर खड़ी मिले। घर में काम करने वाली भी अब नसीब वालों को मिलती है! बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं वे खुद को एक कंफ्यूजन की स्थिति में पाते हैं। पहले बच्चे सिर्फ घर और स्कूल तक सीमित थे। आसपास उनके दोस्त होते थे और वे सभी एक ही तरह कि आर्थिक-सामाजिक स्थितियों वाले होते थे। जेनरेशन गैप कम था। अब हालात बदले हुए हैं। अब मीडिया, इंटरनेट और टीवी के चौतरफा हमले से बच्चे खुद को कई तरह के मूल्यों के रूबरू पाते हैं। उनपर असर डालने वाले सिर्फ उनके मां-बाप नहीं, बल्कि कई और स्रोत हैं। यदि मां-बाप का मुख्य कार्य बच्चों को संस्कारित करना है तो देखा जाए तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अर्थ में अब बच्चों के कई मां-बाप होते हैं, जो उन्हें अपने-अपने ढंग से संस्कारित करते हैं। ऐसे में बच्चों के जैविक माता पिता की भूमिका अब पहले की तुलना में काफी सीमित हो गयी है लगता है।
मदर्स डे, फादर्स डे, फलाना डे में बाजार की बड़ी दिलचस्पी होती है। यह प्रभाव मुख्य रूप से पश्चिम से आया है जहां मां-बाप और बच्चों को एक-दूसरे से मिलने के लिए भी पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वहां खासतौर पर एक दिन इस तरह के रिश्तों का उत्सव मनाने के लिए तय कर दिया जाता है। फिर बाजार ऐसे मौकों को भुनवाने के लिए टूट पड़ता है। जब आर्चीज और हॉलमार्क के कार्ड्स नहीं थे, टेडी बेयर नहीं थे, तो प्यार का इजहार कैसे होता था? एक दूसरे को भौतिक उपहार देना तो अक्सर प्यार और समय न दे पाने की अवस्था की क्षतिपूर्ति होती है। वरना संबंधों में ट्रांजेक्श्न की क्या जरूरत? संबंधों में तो हर दिन एक उत्सव है, रोज एक दूसरे की फिक्र है, रोज एक दूसरे को समय देना होता है, न कि बाजार द्वारा तय किए गए किसी खास दिन एक दूसरे पर प्यार उड़ेलने को लोग मचलने लगते हैं। मानवीय भावनाएं किसी खास दिन उमड़ें और वह दिन हर वर्ष पहले से ही तय हो, ऐसा नहीं होता। सिर्फ उत्पादन, उसकी मात्रा, उसका लक्ष्य और उसके बेचने के दिन तय हो सकते हैं, और इस तरह के सभी दिन बाजार के लिए जश्न के दिन होते हैं, जीवन के ठोस यथार्थ से उनका कोई संबंध नहीं होता। मां, बाप, प्रेम, टीचर्स वगैरह के नाम पर दिन तय होते हैं और चांदी काटता है बाजार।